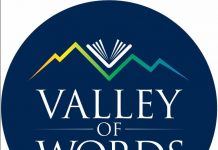उत्तराखंड राज्य बनते ही देहरादून को कामचलाऊ राजधानी बना दिया गया। कुछ लोगों ने इसका विरोध किया और आज भी गैरसैंण को राजधानी बनाने की लड़ाई जारी है। राजधानी को देहरादून से हटाने का मुद्दा भी हर अन्य मुद्दे की तरह राजनीतिक ज़्यादा और व्यावहारिकता से दूर हो गया। जो नेता इस पर राजनीतिक रोटियाँ सेक रहे हैं वो तमाम तरह के कॉस्मैटिक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तो कर रहे हैं लेकिन गैरसैंण में राजधानी बनाने को लेकर ज़मीनी तैयारी क्या है इसके बारे में फ़िलहाल कोई जानकारी शायद ही किसी के पास है। ख़ुद मुख्यमंत्री ये कह चुके हैं कि ये काम “शनै शनै” यानि धीरे धीरे ही होते हैं लेकिन ये धीरे कितना धीरे होगा ये शायद चुनावों के नतीजे तय करेंगेँ। वहीं जो लोग राजधानी शिफ़्ट करने के पक्षधर हैं चाहे वो राज्य आंदोलनकर्मी हो या बेतरतीब “विकास” से परेशान हो चुके देहरादून के लोग वो भी न ये समझ पा रहे हैं न समझा पा रहे हैं कि जिस राज्य को अपने मासिक ख़र्चे चलाने के लिये केन्द्र सरकार पर निर्भर रहना पड़ रहा है उसपर एक नई राजधानी को बनाने का बोझ डालना कितना सही होगा। सिर्फ़ घोषणा करने से गैरसैंण में राजधानी तो नहीं बन पायेगी। एक समाधान इस मुद्दे का ये भी है कि जम्मू कश्मीर की तर्ज पर गैरसैंण को समर कैपिटल (गर्मियों की राजधानी) बना दिया जाये। सुनने में ये बात और मौजूद समाधानों से ज्यादा व्यवहारिक लगती है मगर सवाल फिर वही है कि क्या कर्ज के बोझ तले दबे राज्य पर दो राजधानियों का भार डालना तर्क संगत होगा। ये भी तय है कि अगर ऐसा होता है तो गैरसैंण में लोगों के लिये मूलभूत सुविधायें आये या नहीं लेकिन नेताओं और अधिकारियों के लिये आराम से रहने और काम करने का इंतजाम पहले किया जायेगा। ऐसे में आम लोगों को क्या हासिल होगा राजधानी गैरसैंण ले जा कर।
इन सब राजनीतिक और सामाजिक खिंचातनी के बीच जो हारा है वो है देहरादून शहर। पिछले एक दशक में विकास के नाम पर देहरादून में तक़रीबन सबकुछ बदल गया है। गलियों मे इमारतें खड़ी हो गई हैं, संकरी सड़कों पर देसी विदेशी गाड़ियाँ दौड़ने लगी हैं, डिमांड से ज़्यादा मकानों की सप्लाई बन गई है, किसी ख़ास कारण के चलते यहाँ के निवासी पलायन कर रहे हैं और बाक़ी सब जगह से लोग यहां आकर बस रहे हैं। पलायन भी एक राजनीतिक मसला और सेमिनारों का ज्वलंत मुद्दा बनकर रह गया है लेकिन पहाड़ों से हो रहे पलायन के मूल कारणों और इसे रोकने के लिये कोई भी राजनीतिक दल या सामाजिक संगठन कुछ ठोस कर पाया हो ऐसा नहीं दिखता। किसी भी शहर के लिये ये सब फ़ैक्टर शायद विकास के पैमाने माने जायेंगे, पर यहाँ सवाल ये है कि क्या सही मायनों मे इसे विकास कहेंगे आप?
क्या हम ये भी सोचेंगे कि वास्तविकता में हमें इस तरह हो रहे “विकास” की ज़रूरत है? पिछले दस सालों में शहर में सरकारी नौकरियों के अलावा और नौकरियों के कितने मौक़े बनाये गये? सचिवालय में जितनी फाइलें कामों की होती हैं तकरीबन उतनी ही “आर्थिक सहायता” की अर्जियां उन्हें मुकाबला देती दिखती हैं। क्यों ऐसा हो गया है कि हमारे राज्य के हर वर्ग के लोग विकास के अवसरों की जगह मुख्यमंत्री राहत कोश की तरफ ज्यादा देखने लगे हैं। क्या ये अरेंजमेंट हमारे राजनेताओं को भी वोटर मैंनेजमेंट करने में ज्यादा कारगर दिखता है। राज्य बनने के बाद से ज़मीनी और ज़रूरी इंफ़्रास्ट्रक्चर बनाने के लिये क्या क़दम उठाये गये हैं? शहर में गाड़ियाँ तो हो गई हैं लेकिन सड़के नहीं, इमारतें तो बन गई हैं लेकिन सीवेज की लाइनें नहीं, मॉल हैं लेकिन ग्राहक नहीं है।
उत्तराखंड राज्य का निर्माण आंदोलन की राह पर चल कर हुआ था और वो आंदोलन और उसमें दिया गया बलिदान हमारी सांस्कृतिक विरासत का अमिट हिस्सा बन गया है। लेकिन इस समय की ज़रूरत है कि राज्य को धरना प्रदर्शन राज्य की छवि से मुक्त कराया जाये और सब लोग एक साथ आकर राजनीतिक खेल की सबसे पुरानी चाल जात पात, धर्म, भूगौलिक भिन्नता को दरकिनार कर अपने नेताओं की जवाबदेही तय करें। हम कहीं न कहीं इस मानसिकता के शिकार हो गये हैं कि हर राजनेता एक समान है और हमारी मजबूरी है इन्हें चुनना। लेकिन जब हम अपने घर के लिये सामान खरीदते हुए समझौता नहीं करते तो हम अपने राजनेताओं को चुनते समय समझौता कैसे कर सकते हैं।
शायद अब ये समय आ गया है कि देहरादून के बाशिंदे अपने हुक्मरानों से सवाल जवाब करने लगें वरना कुछ दिन पहले ही हमने आँख बंदकर हुए “विकास” के नतीजों का ट्रेलर दिल्ली और एनसीआर की हवा में देख चुके हैं।