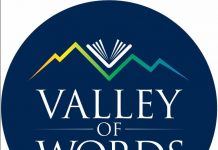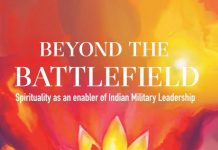लेफ्ट पार्टियों के सिकुड़ने और खारिज होने का ताजा प्रमाण यह है कि अब इनका पश्चिम बंगाल से कोई भी सदस्य राज्य सभा में नहीं आयेगा। राज्यसभा के इतिहास में आजादी के बाद यह पहली बार हो रहा है। वैसे तो लेफ्ट पार्टियों का पतन भारतीय राजनीति के लिए शुभ संकेत नहीं है। इन दलों को अब अपनी वजूद को कायम रखने के लिए जनता के बीच में अधिक काम करना होगा। जनता से जुड़े मुद्दों पर संघर्ष करते रहना होगा। इन्हें देश के राजनीतिक पटल से पूरी तरह से खारिज होने से अपने को बचाना ही होगा।
जनभावनाओं की अनदेखी
आप वाम दलों के पतन का गहराई से अध्ययन करें तो महसूस करेंगे कि इन दलों का नेतृत्व पिछले पचास दशकों से जन भावनाओं से पूरी तरह से हटकर सोच रहा है। इसका एक उदाहरण ले लीजिए। यह बहुत पुरानी बात नहीं है जब केन्द्र सरकार ने कहा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक किया और वहां आतंकियों के ठिकानों को नष्ट किया। जवाब में ये वाम दल मांग करते रहे कि सरकार सर्जिकल स्ट्राइक के प्रमाण प्रस्तुत करे। वामदल अपने को गरीब-गुरबा के हितों का सबसे मुखर प्रवक्ता बताते हैं। जरा कोई बता दे कि इन्होंने हाल के वर्षों में कब महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी जैसे सवालों पर कोई आंदोलन छेड़ा हो। सारा देश राष्ट्रीय एकता और अखंडता के सवालों पर एक है। इस पर भी ये वामदल अपने तरीके से सोच रहे हैं। इनके येचुरी तथा करात सरीखे नेता सिर्फ कैंडिल मार्च निकाल सकते हैं या केरल में आर.एस.एस. के कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या पर वामपंथी कार्कर्ताओं के बचाव में खड़े हो सकते हैं। इसीलिए अब इन्हें जनता खारिज करती जा रही है। देश ने 1962 में चीन से जंग के वक्त इनका पहली बार असली चेहरा देखा । तब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी(भाकपा) ने राजधानी के बारा टूटी इलाके में चीन के समर्थन में एक सभा तक आयोजित करने की हिमाकत की थी। हालांकि वहां पर मौजूद लोगों ने तब आयोजकों को अच्छी तरह पीट दिया था। इसके अलावा वामदलों के अधिकतर राज्यों में सिकुड़ने का एक अहम कारण यह भी है कि इनके गैर जिम्मेदाराना हरकतों से छोटी-बड़ी फैक्ट्रियां बंद होती रही हैं। इसके चलते वामपंथी ट्रेड यूनियन आंदोलन कमजोर हो गया और वाम नेता दूसरे किसी मुद्दे पर कोई विशेष छाप नहीं छोड़ सके। संगठन के स्तर पर भी इन्होने कोई जमीनी काम नहीं किया, सिवाय इसके कि फर्जी एन.जी.ओ. बनाकर सरकारी योजनाओं का पैसा कांग्रेस के सहयोग से भरपूर लूटा और हर तरह की मौजमस्ती में अपना समय और लूट के धन का अपव्यय किया।
घटा स्पेस
कुछ महीने पहले हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के चुनाव के नतीजों ने स्पष्ट कर दिया कि लेफ्ट पार्टियों के लिए देश की राजनीति में अब कोई स्थान नहीं रह गया है। अप्रासंगिक होती जा रही वामपंथी पार्टियों की नीतियों और कार्यक्रमों को जनता स्वीकार करना तो छोड़िए, सिरे से ही ख़ारिज करती जा रही है। इसीलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) लोक सभा से लेकर राज्य विधानसभा चुनावों तक में धराशायी होती जा रही हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव में पहली बार भाकपा, माकपा और भाकपा( माले) ने विधानसभा चुनावों के लिए साझा प्रत्याशी उतारे। उन्होंने सौ सीटों पर कम से कम 10 से 15 हजार वोट हासिल करने का लक्ष्य रखा।
वामदलों से सीताराम येचुरी, डी.राजा, वृंदा करात, दीपांकर भट्टाचार्य जैसे नेताओं ने जमकर प्रचार किया। फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। आंकड़े गवाह हैं कि करोड़ों की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में वामदल कुल मिलाकर एक लाख 38 हजार 763 वोट ही हासिल कर सके। यह कुल मतों का दशमलव दो प्रतिशत होता है। वहीं नोटा के लिए प्रदेश की जनता ने सात लाख 57 हजार 643 वोट दिए, यह करीब दशमलव नौ फीसदी बैठता है।
कभी वाम मोर्चा का गढ़ रहे पश्चिम बंगाल में भी उसकी दुकान बंद होती जा रही है। वहां 2011 के विधानसभा चुनाव में उसे 41.0 फीसद मत मिले। यह आंकड़ा 2014 के लोकसभा चुनाव में 29.6 फीसद रह गया। अब आया 2016 का विधानसभा चुनाव। अब लेफ्ट पार्टियों को मिले 26.1 फीसद। यानी गिरावट का यह सिलसिला लगातार जारी है। गौर करें कि पश्चिम बंगाल में जैसे-जैसे लेफ्ट पार्टियां सिकुड़ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी का असर वहां पर उसी रफ्तार में बढ़ता जा रहा है।
नौजवानों की ना
अब ये पार्टियां पश्चिम बंगाल, केरल तथा त्रिपुरा में ही सिकुड़ कर रह गई हैं। इनसे अब नौजवान नहीं जुड़ पा रहे हैं। माकपा के कुल सदस्यों में मात्र 6.5 फीसद ही 25 साल से कम उम्र के हैं। माकपा का नेतृत्व तो बुजुर्गों से भरा है। नेतृत्व में नौजवान नाममात्र के ही हैं। माकपा की एक ताजा रिपोर्ट में बताया गया है कि उसकी विशाखापट्नम में 2015 में हुई कांग्रेस में 727 नुमांइदों ने भाग लिया। उनमें सिर्फ दो ही 35 साल से कम उम्र के थे। यानी माकपा से नौजवानों का मोहभंग होता जा रहा है। अब माकपा और पश्चिम बंगाल की बात कर लीजिए। बंगाल पर माकपा ने 1977 से लेकर 2011 तक राज किया। ज्योति बसु लंबे समय तक माकपा के नेतृत्व वाली वाम सरकार के मुख्यमंत्री थे। अब उसी बंगाल में भी माकपा लोकसभा और राज्य सभा के चुनाव बार-बार हार रही है।
फिर वापस चलते हैं उत्तर प्रदेश चुनाव पर। तब ये पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक चंद वोटों को ही जुटाने में तरस गए। अयोध्या की बात करें तो यहां भाकपा के सूर्यकांत पांडेय काफी कोशिश के बाद भी महज 1353 लोगों का ही वोट हासिल कर सके। दंगे की आग से झुलसे मुजफ्फरनगर में माकपा के मुर्तजा सलमानी को कुल मिलाकर 491 वोट ही मिले। आजमगढ़ में भी यही हाल रहा। यहां माकपा के राम बृक्ष की 1040 वोट के साथ जमानत जब्त हुई, जबकि गाजियाबाद के साहिबाबाद में इसी पार्टी के जगदंबा प्रसाद 1087 वोट के साथ जमानत नहीं बचा सके। इन सभी जगहों पर वाम दलों का बीते समय में तगड़ा असर रहा है। यानी उत्तर प्रदेश से लेफ्ट पार्टियां का सूपड़ा साफ हो चुका है। 2007, 2012 के बाद अब 2017 में वह एक सीट जीतने को तरस गए।
हो सकता है कि आज की पीढ़ी को मालूम न हो, पर एक दौर में उत्तर प्रदेश में वाम दलों का असर था। 1957 से 2002 के बीच हुए विधानसभा चुनावों में वाम दल के उम्मीदवार जीत हासिल करते रहे। इनमें 1969 की भाकपा की 80 और माकपा की एक सीट पर जीत अब तक की वाम दलों की उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जीत मानी जाती है।
केरल में वाम दलों का एक अलग चेहरा भी देश देख रहा है। वहां पर इनकी सरकारों के संरक्षण में गुंड़े बीते दशकों से भाजपा और आरएसएस के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार रहे हैं। अभी तक सैकड़ों कार्यकर्ता मारे जा चुके हैं। इसके बावजूद वहां की बेशर्म सरकारें खूनियों को बचाती रही हैं। सारा देश देख रहा है केरल में खेले जा रहे इस खूनी खेल को। निस्संदेह इन तमाम कारणों के चलते ही देश का मतदाता वाम दलों की चुनावों में भरपूर दुर्दशा कर रहा है।